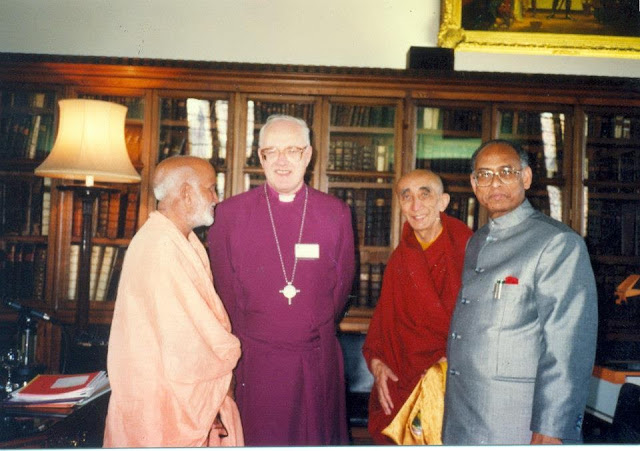भूमिका
किधौं सूर कौ सर
लग्यौ, किधौं
सूर की पीर ।
किधौं सूर को पद लग्यौ,
तन मन धुनत सरीर ।।
कृष्णकाव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के संबंध में
कथा प्रचलित है कि एक बार सूरदास और तानसेन की भेंट हो गई। तानसेन ने सूरदास
द्वारा गाए जा रहे पद को तन्मयता के साथ सुना और एक सहृदय श्रोता का भावनात्मक-संवेदनात्मक
जुड़ाव एक भक्तकवि से हो गया। कला के पारखी के लिए शील साँसों के उतार-चढ़ाव की
तरह होता है और विनम्रता शरीर की भाँति। इसी कारण संगीत सम्राट तानसेन के अंतर्मन
से पंक्तियाँ प्रस्फुटित हो उठीं। तानसेन कह उठे कि जब किसी तड़पते हुए व्यक्ति को
देखता हूँ, तो लगता है कि शायद इसे किसी शूर (योद्धा) का बाण लग गया है अथवा इसे
उदर-सूर (शूल) की बीमारी हो गई है या फिर निश्चित ही सूर का कोई पद इसके लग गया
है। इसी कारण यह व्यक्ति तड़प रहा है। वस्तुतः यह तड़प संगीत सम्राट तानसेन की ही
रही होगी, जो शब्दबद्ध होकर सूरदास की महिमा का गान करने लगी। सूरदास भी कला के
पक्के पारखी थे, इसी कारण अकबर के नवरत्न तानसेन की वाणी को सुनकर तुरंत ही कह
उठे-
बिधना यह जियँ जानि कै, सेसहि दिये न कान ।
धरा मेरु सब डोलि हैं,
तानसेन की तान ।।
भक्तकवि सूरदास कह उठते हैं कि विधाता ने यह जान-समझकर
शेषनाग को कान नहीं दिए हैं कि यदि तानसेन के गाने को, तानसेन की तान को शेषनाग
सुन लेगा; तो उसके थिरक उठने से धरती और मेरु पर्वत, सभी डोलने लगेंगे।
सूर के पदों में गुँथे हुए संगीतशास्त्र के कोमल तंतुओं ने
संगीत सम्राट तानसेन को ऐसा कसकर बाँध लिया कि तानसेन के मुख से बरबस ही सूर के पद
निकल पड़ते थे। ऐसे ही एक बार अकबर के सामने तानसेन सूरदास का एक पद गा उठे। बादशाह
उस पद की सरसता पर मोहित हो गए। उस पद को सुनकर अकबर ने सूरदास से मिलने की इच्छा
प्रकट कर दी। तानसेन ने सूरदास से अकबर की भेंट करा दी। अकबर की सहृदयता से
प्रभावित होकर सूरदास ने एक पद अकबर को सुनाया। अकबर ने पद सुनने के बाद कहा कि
जिस तरह कृष्ण के यश को गाया है, उसी तरह मेरे भी यश को गाएँ। इस पर सूरदास गाने
लगे कि मेरे हृदय में तो केवल नंदनंदन ही बसे हैं और इस कारण मेरे हृदय में किसी
दूसरे के बसने का स्थान ही नहीं है। तब मैं आपका यश कैसे गाऊँ?
नाहिन रह्यो हिय महँ ठौर । नंदनंदन अछत आनिए डर और ।।
‘चौरासी वैष्णवन की वार्ता’ में अकबर और सूरदास की भेंट का
वर्णन मिलता है। इसमें गोसाईं हरिराय उल्लेख करते हैं कि यह भेंट तानसेन ने संवत्
1633 (सन् 1576 ई.) के आसपास कराई थी। कई विद्वान इस घटना की सच्चाई को स्वीकार
नहीं कर पाते हैं। भले ही यह घटना ऐतिहासिक न हो, मगर लोकपरंपरा में प्रचलित इस
किंवदंती पर पूरी तरह से अविश्वास कर लेना भी उचित नहीं है। यहाँ प्रश्न इस घटना
की सत्यता को जाँचने का नहीं है, प्रत्युत् इसके माध्यम से कृष्णकाव्य परंपरा के
प्रतिनिधि कवि सूरदास के कृतित्व और व्यक्तित्व की महानता को देख लेने का है।
सूरदास के प्रति तानसेन का निर्मल-पवित्र अनुराग, तानसेन की
सूरदास के प्रति विनम्रता और आस्था ही उस कारण को जन्म दे सकी, जिससे सूरदास ने
तानसेन के संदर्भ में ‘नाहिन रह्यौ हिय महँ ठौर’ नहीं कहा, वरन् शेषनाग को भी नचा
देने वाली तान छेड़ने वाले संगीत-साधक तानसेन कहकर महिमामंडित कर दिया। यह प्रीति,
यह जुड़ाव भय के कारण नहीं, वरन् आत्मीय संबंध के कारण है, जो आत्मा के काव्य के
साथ आत्मा के संगीत को जोड़ता है। सूरदास आत्मा की बात को आत्मा से कहने वाले ऐसे
विरले कवि हैं, जो अंतर्मन की गहराई में उतरकर शब्दों को जिह्वा तक लाते हैं और
वीणा की सुरीली-मधुर झनकार के साथ मिलाकर एक ओर बाह्यजगत् को उद्वेलित कर देते
हैं, तो दूसरी ओर अंतर्मन के तारों को झंकृत करके बुद्धि को निर्मल और प्राण को
पुलकित कर देते हैं। अंतर्मन से बाह्यजगत् तक की यह वृत्ताकार गति उस मोक्ष तक पहुँचा
देती है, जिसकी प्राप्ति की कामना साधारण मानव से लेकर साधक तक को होती है।
कृष्णकाव्य परंपरा का विस्तार लगभग सारे देश में रहा है और
विभिन्न संप्रदायों के भक्तकवियों ने कृष्णकाव्य परंपरा को समृद्ध किया है। वल्लभ
संप्रदाय (श्री वल्लभाचार्य, तेलुगु), चैतन्य संप्रदाय (चैतन्य महाप्रभु, नवद्वीप,
बंगाल) और राधावल्लभ संप्रदाय (श्री हित हरिवंश) का आश्रय लेकर कृष्णकाव्य परंपरा विकसित
हुई। उस समय बने नैराश्य के वातावरण के कारण बहुसंख्य जनता में जीवन के प्रति
जागृत हो गई विरक्ति को नष्ट करके जीवन के प्रति अनुराग जगाने का काम इस पंरपरा के
कृष्णभक्त कवियों ने किया। सूरदास इस परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं,
किंतु सूरदास ने एकदम अलग ही रास्ता बनाया, जहाँ ब्रजभाषा में कृष्ण-भक्ति, काव्य
और संगीत की त्रिवेणी का दर्शन होता है; जहाँ प्रेम, भक्ति और अध्यात्म एक-दूसरे
से मिल जाते हैं और आराधक-आराध्य का भेद भी नहीं रह जाता है।
सूर की एक अन्य विशिष्टता है- गृहस्थ जीवन और परिवार के
चित्रों को उकेरना। रामायण और महाभारत के केंद्र में भी परिवार हैं। वहाँ
राजपरिवारों के संघर्ष का यथातथ्य चित्रण क्रमशः नीति-नैतिकताओं और मर्यादों को
विश्लेषित करता है। परिवार सूरदास के मुक्तक पदों में भी है, मगर वह सामान्य किसान
का परिवार है। वहाँ नंद, यशोदा, कृष्ण और बलराम हैं। वहाँ परिवार के साथ जीवनधारा
बनकर चलता गौवंश है, नेह-प्रेम में डूबे हुए गोप हैं, गोपियाँ हैं और राधिकाजी
हैं। वहाँ परिवार के संघर्ष नहीं, आस-पड़ोस के झगड़े-टंटे नहीं, वरन् कन्हैया की
बाललीलाएँ हैं, खेल हैं, हँसी-ठिठोलियाँ हैं, रार-मनुहार हैं और भोले-भाले-से
ताने-उलाहने हैं। आगे चलकर वियोग के पक्ष के साथ सूरदास उतने ही ज्यादा दार्शनिक
हो जाते हैं; जितना बचपना, जितनी खिलखिलाहट वे कृष्ण के बचपन की बिखेरते हैं।
परिवार के माध्यम से चलते हुए तब ऐसा प्रतीत होता है, मानों वे एक छोटे-से परिवार
के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए किसी बड़े परिवार की जिम्मेदारी को निभाने में
लग गए हों- निर्गुनिया, निरंजनी, नाथपंथी साधुओं और आक्रांताओं के धर्म से
भागवत-भक्ति को बचाने की। आचार्य वल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्ग को अपनी वीणा
की सुरीली और मधुर झंकार से प्रसृत करके सूरदास ने जिस तरह सगुणोपासना के मार्ग को
प्रशस्त किया है, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है।
एक प्रसंग आता है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित चौरासी
वैष्णवन की वार्ता में; कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य मथुरा के गऊघाट में कुछ
दिनों के लिए टिके थे। वहीं पर सूरदास का निवास भी था। सूरदास को जब वल्लभाचार्य
जी के आगमन का पता चला, तो वे मिलने पहुँच गए। उस समय वल्लभाचार्य जी भोजन ग्रहण
करके गद्दी में विराजमान थे। वल्लभाचार्य जी ने भी सूरदास की प्रशंसा सुन रखी थी,
इस कारण उन्होंने कोई पद गाने के लिए कहा। सूरदास ने ‘हरि हौं सब पतितन कौ
नायक...’ गाया। बाद में ऐसे ही कुछ अन्य भजन भी सुनाए। सूरदास के पद सुनकर
वल्लभाचार्य जी ने कहा कि- ‘सूर ह्वै कै ऐसों घिघियात काहै कों हौं, कछू
भगवत्-लीला वर्णन करि।’ सूरदास ने इस पर अपनी अज्ञानता प्रकट की। उसी समय महाप्रभु
ने उन्हें दीक्षित करके श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध का प्रवचन दिया। इसके बाद
दास्यभाव को तजकर सूरदास सख्यभाव के, वात्सल्य-भाव के पद रचने लगे। तुलसीदास की
भक्ति दास्यभाव वाली है। उपास्य और उपासक के मध्य जितनी रिक्तता तुलसी की रचनाओं
में मिलती है, उतनी ही सघनता उपास्य और उपासक के बीच सूरदास के पदों में मिलती है।
सख्यभाव और वात्सल्य-भाव सूरदास को जितना आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न बनाते हैं,
उतना अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। इसी कारण लोकव्यवहार में प्रचलित है कि-
तत्त्व तत्त्व
सूरा कही, तुलसी
कही अनूठी ।
बची-खुची कबिरा कही, और कही सो जूठी ।।
आत्मा के काव्य के सर्जक, लोक-रंजना के आराधक और काव्याकाश
में सूर्य की भाँति अपने अध्यात्म के प्रकाश से आलोकित होने वाले भक्तकवि सूरदास
की ख्याति भौगौलिक बंधनों और काल की सीमाओं से परे है। उनकी सर्जना हर युग में,
प्रत्येक कालखंड में जीवन जीने की ऊर्जा देने वाली है और जीवन की नकारात्मक
शक्तियों को पराजित करने की सामर्थ्य भी रखती है। आज के जटिल जीवन में भक्तकवि
सूरदास का स्मरण इसी कारण प्रासंगिक है। साहित्य की विविध धाराओं और नवसृजित
विषयों-चिंतनधाराओं-वैचारिकताओं के बीच सूरदास को स्मरण कराने का यह प्रयास
निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रेरणा के कारण ही संभव हो सकता है, और इस हेतु पुस्तक
के संपादक डॉ. अशोक मर्डे अशेष साधुवाद के पात्र हैं। हिंदी की सेवा के लिए उनका
यह अवदान कभी विस्मृत नहीं होगा।
डॉ. राहुल मिश्र
(कृष्णकाव्य के महाकवि : सूरदास, संपादक- डॉ.
अशोक मर्डे, प्रकाशक- शिल्पा प्रकाशन, शिव-कांची, बिदर रोड, उदगीर- 413 517 की
भूमिका)