शयोक! तुम्हें पढ़ा जाना अभी शेष है...
कहते हैं, पहाड़ी नदियाँ बड़ी शोख़ होती हैं, चंचल होती
हैं। लहराना, बल खा-खाकर चलना ऐसा, कि
‘आधी दुनिया’ को भी इन्हीं से यह हुनर सीखना पड़े। पहाड़ी नदियाँ तो बेशक ऐसी ही
होती हैं, मगर कभी हिमानियों से अपना रूप और आकार पाने वाली नदियों के बारे में
सोचा है? वैसे तो ये भी पहाड़ों की ही हैं। इसलिए शोख़ी और चंचलता, बाँकपन और
अदाकारी इनमें नहीं होगी, ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता है। देख लीजिए अलकनंदा और
भागीरथी को, देख लीजिए लोहित और असिक्नी को....., और इनकी जैसी अनेक नदियों को....।
एक अलग-सा सौंदर्य, अनूठा अल्हड़पन इनमें नजर आएगा। हिमनदों की इन आत्मजाओं का
अनूठा सौंदर्य हिमालय की ऊँचाइयों पर ही देखा जा सकता है। अपने उद्गम से आगे बढ़ते
हुए इनकी चंचलता मैदानों तक पहुँचते-पहुँचते गंभीरता में बदल जाती है। ठीक बचपन और
बुढ़ापे की तरह...।
हिमनदों की इन चंचल बेटियों में एक शयोक भी है, जो अपनी
कुछ अलग ही तासीर रखती है। यह चंद्रा और लोहित की तरह, अलकनंदा की तरह, या फिर
भागीरथी की तरह सीधी-सरल और शांत नहीं है। लेह की तरफ से खरदुंग दर्रे को पार करते
ही जैसे हम नुबरा घाटी में पहुँचते हैं, हरहराती हुई और तेजी से भागती हुई शयोक
जैसे अगवानी करने को तैयार मिलती है। नुबरा घाटी में हम जितने दिन गुजारते हैं,
उतने दिनों तक शयोक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। नुबरा घाटी में घूमते हुए कई-कई बार
हमें इसके साथ, तो कई बार इसे पार करके दर्शनीय स्थलों में पहुँचना होता है। इतना
ही नहीं, शयोक अपने प्रवाह के साथ अपनी एक उपघाटी या अपना मैदानी इलाका भी बनाती
है।
अल्हड़ शयोक अपने उद्गम स्थान से निकलकर ‘गप्शन’
तक पश्चिम और दक्षिण तक बहती है और ‘गप्शन’ से ‘मंदरालिङ’ तक पूर्व दिशा में बहती है। अपने उद्गम से आगे निकलकर यह गलवाँ और
चंङ छेनमो नदियों को अपने साथ ले लेती है। इसके साथ ही यह इस इलाके में मंगोलियन
तिब्बत और लद्दाख के बीच एक प्राकृतिक विभाजक रेखा भी खींचती है। ‘मंदरालिङ’ से ‘शयोग’ तक दक्षिण और ‘शयोग’ से
‘हुंदर’ तक पश्चिमोत्तर बहते हुए बाद में पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए बल्तिस्थान
में प्रवेश कर जाती है। बल्तिस्थान के प्रमुख शहर स्करदो के पूर्व की ओर स्थित
‘केरिस’ के नजदीक सिंधु से मिल जाती है।
कई-कई बार शयोक की अल्हड़ चाल को देखकर ऐसा लगता है, जैसे
वह ‘खरदुंग-ला’ से बहुत नाराज हो। ‘खरदुंग-ला’, यानि खरदुंग दर्रा....भोटभाषा में
‘ला’ दर्रे को कहते हैं। ‘ला’ तो ठीक है, लेकिन ‘खरदुंग’ तो ‘खर’ और ‘तुंग’ का
मिश्रण समझ में आता है, जो प्रजातियों-पीढ़ियों की जुबानों में घिस-घिसकर ‘खरदुंग’
हो गया है, शायद। एकदम खड़ी-सी, ऊँची और कठिन चढ़ाई वाला तुंग....खरतुंग। आखिर
यह शयोक के रास्ते में आया ही क्यों? उत्तर आसान-सा है, सरल-सा ही है...। पहाड़
हमेशा धीर-गंभीर और वीरव्रती ही नहीं होते, ये खलनायक की भूमिका में भी कभी-कभी आ
जाते हैं। ऊँचे-ऊँचे दुर्गम और कठिन दर्रों के कारण ही लदाख के लिए कहा जाता है,
कि यहाँ पर बहुत घनिष्ठ मित्र या बहुत कट्टर दुश्मन ही पहुँच सकता है। मध्यम स्तर
वालों के लिए यहाँ आना सुगम नहीं...संभव नहीं। कारण... पहाड़ ही यहाँ पर चुनौतियों
के द्वार खोलते हैं। शायद इसी कारण शयोक
की कथा में खरदुंग-ला किसी खलनायक से कम नजर नहीं आता। ऐसी ही एक कथा लाहुल-स्पीति
के लोककंठों में जीवंत मिलती है। इस कथा में बारालाचा की दुर्गम ऊँचाइयाँ चंद्रा
और भागा के लिए अवरोधक बनती हैं।
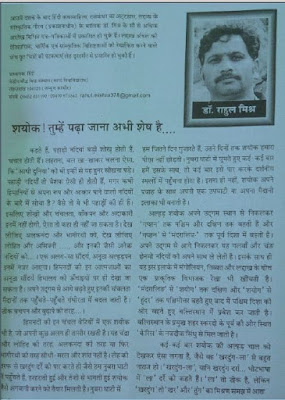
यही अमर प्रेम शयोक और सिंधु में भी तो दिखता है, इसी कारण
मिलन की राह में खड़े खर-तुंग से नाराज शयोक एकदम अपनी दिशा बदलकर बहने लगती है।
इसीलिए खरदुंग-ला के पदतल में, हमें जैसे ही शयोक के दर्शन होते हैं, उसका भर्राया
हुआ गला, नाराजगी से भरा स्वर सुनाई देता है। नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों में
स्वयं को देखने की, मानवीय गुणों और प्रवृत्तियों को देखने की अनूठी भारतीय पंरपरा
दुनिया में विलक्षण है, अद्भुत है। इसी कारण शयोक के ही नहीं, हमारे अपने स्वर भी
दो प्रेमियों के मिलन की राह में बाधक बनने वाले खलनायक खरदुंग-ला के लिए नाराजगी से
भर जाते हैं। बारालाचा में अगर सूरज का बेटा है, तो यहाँ रिमो हिमानी की बेटी है।
उधर चंद्रा है, जो बड़ी शालीन और संयत है। इधर शालीनता सिंधु नद के हिस्से में है।
वैसे ‘रिमो’ भी भोटभाषा का शब्द है, और धारीदार पहाड़ के लिए इसे प्रयोग किया जाता
है। जब माई ही इतनी तीखी है, तो बिटिया शांत-संयत कैसे हो सकती है? कई बार यह
विचार शयोक की अल्हड़ चाल के कारणों को खोजते समय मन में उतर पड़ता है।
वैसे शयोक को कुछ और करीब से जानना हो, तो पाँच-छः घंटे का
समय निकालकर स्याम गोनबो की लगभग सात-आठ सौ फीट की ऊँचाई पर चढ़ जाइए। धरती के
टुकड़े को चाकू से काटती तेज धार की तरह शयोक का बहाव दिखाई पड़ेगा। एक तरफ हिमालय
की लदाख पर्वतश्रेणी है, तो दूसरी तरफ काराकोरम पर्वतश्रेणी है। बीच में शयोक है,
दो पर्वतश्रेणियों को एक-दूसरे से जुदा करती हुई। यह विभाजन पहाड़ों की बनावट का
भी है, और बुनावट का भी...रंग भी दोनों के अलग-अलग...चट्टानें भी अलग और मिट्टी भी
अलग। एक तरफ लालिमा है, तो दूसरी ओर कारा जैसी कालिमा...। स्याम गोनबो की ऊँचाई से
शयोक को देखकर मन में सबसे पहला विचार यही
आता है, कि, भला हो... शयोक तुम्हारा! जो तुमने
दोनों श्रेणियों को अलग-अलग कर दिया.... कहीं हम एक ही समझ बैठते, तो आखिर
क्या होता? यह तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें एक गति से चलना नहीं आता है?
हे शयोक! हमने भी स्याम गोनबो की ऊँचाइयों से तुम्हें
निहारा है। केवल निहारा ही नहीं है, तुम्हारे सानिध्य में पाँच-छः घंटे भी बिताए हैं।
सुबह के समय तुम्हारी चाल थमी हुई-सी होती है। उस समय लगता है, कि तुम घुटुरुअन चल
रही हो। कोई भी तुम्हारे पास जा सकता है। सिर पर सूरज के चढ़ते-चढ़ते तुम्हारे
किनारों के रेतीले मैदानों में नमी पसरने लगती है। कई-कई जलधाराएँ उग आती हैं।
साँझ ढलते-ढलते तुम्हारी चाल बहुत तेज हो जाती है। तुम्हारे सहमे-सिकुड़े से
किनारे दूर-दूर तक फैल जाते हैं। रात के अँधेरों में भी तुम्हारी तेजी बनी ही रहती
है, और सुबह-सवेरे फिर वही वीतरागी मद्धिम चाल....। कहीं तुम्हारे नाम के पीछे
तुम्हारी चाल का असर तो नहीं है? अपने ‘ओक’ में, रिमो की गोद में ‘शयन’ कर रहीं
तुम आलसियों की तरह दिन चढ़ने पर जागती हो, और देर हो जाने की बदहवासी में तेजी से
दौड़ लगा देती हो। तुम्हारी दिन-भर की कलाएँ देखकर ही हमारे मन में ऐसे विचार आते
हैं। हो सकता है, दूसरे लोगों के मन में ऐसे विचार आते हों। ‘शय’ और ‘ओक’ के मिलन
से बनने वाले तुम्हारे नाम के पीछे भी यही विचार हो सकते हैं।
वैसे यारकंदी लोग शयोक को इस नाम से नहीं जानते। उनके लिए
शयोक मौत की नदी है। दरअसल, काराकोरम की विकराल ऊँचाइयों से गुजरने वाले रेशम
मार्ग का सहायक मार्ग नुबरा घाटी से जुड़ा हुआ था। लेह को रेशम मार्ग से जोड़ने
वाले इस सहायक मार्ग की यात्रा करते समय यारकंदी व्यापारियों को लगभग बीस बार शयोक
नदी को पार करना पड़ता था। गर्मियों में
तो इसे पार करना असंभव ही होता था, मगर सर्दियों में भी यह कम कठिन नहीं होता था।
अपनी आदत के हिसाब से शयोक एकदम तेजी के साथ बह पड़ती, और यारकंदी व्यापारियों के
कारवाँ में शामिल ऊँटों, घोड़ों, आदमियों तक को बहा ले जाती। शयोक के किनारे रहने
वाले लोग भी इससे कम डरे हुए नहीं हैं। आज तो तमाम साधन हैं, पुल हैं, सड़कें हैं;
लेकिन गुजरे जमाने में लोग बेबसी को ढोते
थे, और वैकल्पिक रास्ते निकालते थे। शयोक के किनारे के कुछ पुराने गाँवों, जैसे
हुंदर, हुंदरी, देस्किद और उदमारू आदि के लोग चमरी मृग की खाल से ‘बिप्स’, यानि
चमड़े की नाव बनाते थे, और उसके सहारे अपनी जान को जोखिम में डालकर शयोक को पार करते थे।
भूरी-मटमैली रंग की इस मौत की नदी से नुबरा-शयोक घाटी के
लोगों की भी खासी नाराजगी है। जिस शयोक को जीवनदायिनी होना चाहिए, उसके विकराल रूप
से आहत लोग अपनी नाराजगी भी बड़ो रोचक अंदाज में व्यक्त करते हैं। आज भी किसी बूढ़े-बुजर्ग से पूछिए, तो वे कहते हैं कि हम
खेती-किसानी के लिए शयोक का पानी लेना नहीं पसंद करते, क्योंकि शयोक हमें जीवन
देने वाली नहीं है। शयोक ने अपनी बाढ़ के उफान में कई बार हमारे तटबंधों की मिट्टी
बहाई है, हमारी फसलों और पेड़-पौधों को बहाया है। इतना ही नहीं, गाँव के गाँव
बहाकर आबादी को मिटाया है। इसलिए हमें शयोक का पानी अपनी फसलों में नहीं डालना है।
ऐसा कहा जाता है कि बल्तिस्थान के यगबो राजवंश की राजधानी
काफलू में भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में शयोक नदी ने काफलू के चंगथंग इलाके को
पूरी तरह नष्ट कर दिया था। यह चंगथंग इलाका मंगोलियन तिब्बत से सटे चंगथंग के
लोगों का था, जो रेशम मार्ग में नमक का व्यापार किया करते थे। इस भीषण तबाही से
आक्रांत लोगों ने उस इलाके को ही छोड़ दिया। इनमें से कुछ लोग ‘छोरबत’ में बस गए
और कुछ लोग नुबरा घाटी से होते हुए लेह के निकट ‘छुशोद’ गाँव में आकर बस गए। छुशोद
में इन लोगों को ‘बल्ती’ के तौर पर जाना जाता है।
वैसे शयोक ने केवल बल्तियों को ही विस्थापित नहीं किया,
वरन् अतीत के तमाम विस्थापनों को, राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक बदलावों को देखा
है, जो इतिहास में आज भी अनजाने हैं, अनछुए और गुमनाम-से हैं। देश के विभाजन के
बाद कारगिल से सड़क मार्ग द्वारा स्करदो तक जाना संभव नहीं रहा। अविभाजित लदाख में
स्करदो की उतनी ही बड़ी भूमिका होती थी, जितनी लेह की..। डोगरा शासकों के समय में
लदाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्करदो होती थी। सिंधु नद स्करदो से गुजरते हुए
केरिस के पास शयोक से मिलता है। केरिस के पास ही शिगर नदी भी सिंधु में मिलती है। यहाँ
त्रिवेणी बन जाती है, संगम बन जाता है। केरिस के निकट ही ऐतिहासिक काफलू शहर है।
अतीत का एक लंबा कालखंड ऐसा भी रहा है, जब सिंधु और शयोक के
दोआब में दरद भाषा का व्यवहार हुआ करता था। कारगिल-खलच़े से लगाकर
स्करदो-गिलगित-हुंजा से होते हुए मंगोलियाई तिब्बत की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा तक
विस्तृत दरदभाषी क्षेत्र अपने अतीत में दरद आर्यों का निवास स्थान रहा है। आज का
बल्तिस्थान अतीत में इसी दरद देश के अंतर्गत ही आता था। आज की धार्मिक-सांस्कृतिक
विविधताओं के बीच प्रजातिगत एकरूपता अतीत के गौरव की साक्षी है। इस दरद देश का
अतीत महाभारत काल से भी जुड़ा है। महाभारत के युद्ध में दरदों ने कौरवों की तरफ से
युद्ध किया था, जबकि किरातों ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। तिब्बती भोटभाषा
में किरातों को ‘मोन’ कहा जाता है। इन्हीं मोन लोगों के कारण लदाख का एक नाम
‘मोनयुल’, यानि मोन लोगों का इलाका भी है। सिंधु के तट पर ‘मोन’ या किरातों की, और
शयोक के तट पर दरदों की आबादी के सहारे सिंधु-शयोक का दोआब महाभारतकालीन राजनीतिक प्रसंगों
का साक्षी बना होगा।
शयोक तो मानव-सभ्यता के विकास की, हिमालय की निर्मिति की
साक्षी भी है। शयोक तांतव संधि-क्षेत्र या ‘शयोक स्यूटर जोन’ के तौर पर हम शयोक के
प्रवाह को जानते हैं। देश-दुनिया में प्रसिद्ध पङ्गोङ झील की निर्मिति भी शयोक के
प्रवाह के कारण हुई। किसी समय टेथिस सागर की लहरों को झेलने वाला शयोक का
प्रवाह-क्षेत्र आज भी परवर्ती जुरासिक काल के जीवों के चिन्हों को अपने में छिपाए
हुए है। सिंधु नद का अतीत भी इसी तरह परवर्ती जुरासिक काल से जुड़ा हुआ है। इस
कारण सिंधु और शयोक से मिलकर सिंधु-शयोक मेखला का निर्माण होता है। इसी कारण सिंधु
से मिलना ही शयोक की नियति बन जाती है। यह मिलन केरिस में होता है। सिंधु और शयोक
के साथ ही शिगर नदी भी केरिस में मिलती है। अपने गौरवपूर्ण अतीत के साथ केरिस ऐसा
संगम बन जाता है, ऐसा जीवंत प्रयाग बन जाता है, जहाँ अतीत के मानव के अस्तित्व का
पहला अध्याय लिखा जाता है। जहाँ सभ्यताओं के अस्तित्व और संघर्ष की गाथाएँ गुनी
जाती हैं। जहाँ धर्मों-रीतियों-नीतियों के टकराव दर्ज होते हैं। जहाँ भूरी-मटमैली
शयोक नदी सिंधु नद से मिलकर अपनी पूर्णता को पाती है, और न पढ़े गए इतिहास के तमाम
पन्नों को बाँचती है, उवाचती है। शयोक! तुम्हें पढ़ा जाना अभी शेष है..।
डॉ. राहुल मिश्र
(हिंदी प्रचार-प्रसार सोसायटी अमृतसर की पत्रिका 'बरोह' के दिसंबर, 2019 अंक में प्रकाशित)



















