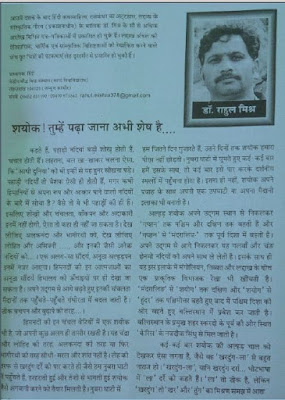यथार्थ के धरातल पर प्रगतिवाद
प्रगति का साधारण अर्थ है- आगे बढ़ना। जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो, वही प्रगतिशील साहित्य है। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो तुलसीदास सबसे बड़े प्रगतिशील लेखक प्रमाणित होते हैं। भारतेंदु बाबू और द्विवेदी युग के लेखक, मुख्यतः मैथिलीशरण गुप्त भी प्रगतिशील लेखक हैं। परंतु आज का प्रगतिवादी इनमें से किसी को भी प्रगतिशील नहीं मानेगा- ये सभी तो उसके अनुसार प्रगतिक्रियावादी लेखक हैं। अतः प्रगति का अर्थ आगे बढ़ना अवश्य है, परंतु एक विशेष ढंग से, एक विशेष दिशा में। उसकी एक विशिष्ट परिभाषा है। इस परिभाषा का आधार है- द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।1
सच्ची बात तो यह है कि
हमारे अधिकांश साहित्यकार, जो प्रगतिवादी वर्ग के नेता माने जाते हैं, स्वयं किसी
पूँजीपति से कम नहीं हैं। पहाड़ियों के वैभवपूर्ण वातावरण में बैठकर निश्चिंतता से
मजदूरों के दुःख-दर्द के गीत लिखे जा सकते हैं, किंतु उनमें अनुभूति की सजीवता आ
जाय, यह आवश्यक नहीं। फलतः प्रगतिवादी साहित्य
हमारे हृदय को बहुत कम स्पर्श करता है।2
हिंदी के जाने-माने
समीक्षक-आलोचक डॉ. नगेंद्र और हिंदी के लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्येतिहासकार डॉ.
गणपतिचंद्र गुप्त के उक्त कथनों के माध्यम से हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद को जाना-समझा
जा सकता है। प्रगतिवाद अपने सीधे-सरल अर्थों में भले ही प्रगति की विचारधारा का
पोषण करने के अर्थ को व्याख्यायित करता हो, किंतु हिंदी साहित्य में जिस रूढ़ और विशिष्ट
अर्थों से संपृक्त प्रगतिवाद की चर्चा की जाती है, वह प्रगति के सीधे और सरल
स्वरूप से पूर्णतः भिन्न है। इसी कारण प्रगतिवाद के सामान्य, सीधे और सरल अर्थ को
ग्रहण कर लेने पर उसी प्रकार की स्थिति का जन्म हो जाता है, जैसी कि हिंदी के
प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत के साथ बन गई थी, जैसी कि प्रेमचंद के साथ बनी थी। डॉ.
नगेंद्र अपने निबंध- ‘प्रगतिवाद और हिंदी साहित्य’ में लिखते हैं-

इस वर्ग के कवि-लेखकों
में केवल एक ही प्रवृत्ति सर्व-सामान्य है- क्रांति। शुद्ध प्रगतिवादी दृष्टिकोण तो
शायद पंत और नये कवियों में नरेंद्र ने ही ग्रहण किया है। और सच तो पंत और नरेंद्र
में भी यह बुद्धि की प्रेरणा, संस्कार अभी उनके पीछे को ही दौड़ रहे हैं। शेष
लेखक-कवि तो अंशतः ही प्रगतिशील हैं।3
अपने इस लेख के उपरोक्त
संदर्भ में नगेंद्र एक टिप्पणी (फुटनोट) भी लिखते हैं- परंतु अब इन दोनों
(सुमित्रानंदन पंत और नरेंद्र शर्मा) को भी प्रगतिवादी पार्टी के चीफ व्हिप डॉक्टर
रामविलास शर्मा ने पार्टी से निकाल दिया है।4 यह टिप्पणी सिद्ध
करती है, कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की पक्षधरता प्रगतिवाद का एक प्रमुख आयाम
कहा जाता है, वह सैद्धांतिक रूप से यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ सुमित्रानंदन
पंत की ‘युगवाणी’ में संकलित कविता ‘चींटी’ के एक अंश को उद्धृत करना प्रासंगिक
होगा। वे लिखते हैं-
निद्रा, भय, मैथुनाहार /
-ये पशु लिप्साएँ चार- / हुईं तुम्हें सर्वस्व-सार? /
धिक् मैथुन आहार यंत्र! /
क्या इन्हीं बालुका भीतों पर / रचने जाते हो भव्य, अमर / तुम जन समाज का नव्य
तंत्र? / मिली यही मानव में क्षमता? / पशु, पक्षी, पुष्पों से समता? / मानवता
पशुता समान है? / प्राणिशास्त्र देता प्रमाण है? /
बाह्य नहीं आंतरिक साम्य
/ जीवों से मानव को प्रकाम्य! / मानव को आदर्श चाहिए, / संस्कृति, आत्मोत्कर्ष
चाहिए, /
बाह्य विधान उसे हैं
बंधन, / यदि न साम्य उनमें अंतरतम- / मूल्य न उनका चींटी के सम, / वे हैं जड़,
चींटी है चेतन! / जीवित चींटी, जीवन वाहक, / मानव जीवन का वर नायक, / वह
स्व-तंत्र, वह आत्म विधायक!/5
यहाँ पंत ने जिस प्रकार प्रगतिवाद
की संकीर्ण वैचारिकता पर तीखी चोट की है, उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता
है कि अपनी तीखी आलोचना को पचा पाना प्रगतिवादियों के लिए सहज नहीं रहा होगा। इसी
प्रकार प्रेमचंद के प्रगतिवादियों से संबंध को व्याख्यायित करना होगा। सज्जाद
ज़हीर के प्रयासों से लंदन में सन् 1935 में स्थापित होने वाला प्रगतिशील लेखक संघ
भारत पहुँचता है। भारत के अनेक साहित्यकारों- जैनेंद्र, गंगानाथ झा, कन्हैयालाल
माणिकलाल मुंशी, सच्चिदानंद सिन्हा, शिवदान सिंह चौहान, नरेंद्र शर्मा, हसरत
मोहानी, जोश मलिहाबादी और डॉ. अब्दुल हक़ सहित रवींद्रनाथ ठाकुर और प्रेमचंद इस
समूह के संपर्क में आए। प्रारंभ में सज्जाद ज़हीर का कहना था, कि यह समूह भारतीय
अतीत की गौरवपूर्ण संस्कृति से उसका मानव-प्रेम, उसकी यथार्थप्रियता और उसके
सौंदर्यतत्त्व लेने के पक्ष में है।6 इस प्रकार प्रगतिवाद की एकदम अलग और प्रायः
सर्वस्वीकृत विचारधारा को लेकर प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 09-10 अप्रैल,
1936 को लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि दो
बैलों की कथा, पूस की रात, आत्माराम, स्वत्व रक्षा, अधिकार चिंता, नागपूजा, पूर्व
संस्कार, सैलानी बंदर, मुक्तिधन, और ऐसी ही तमाम कहानियों के साथ ही उपन्यासों में
प्रेमचंद जितने पशु-पक्षियों के प्रति सहृदय प्रतीत होते हैं, उतना ही लगाव और
आकर्षण भारत के ग्राम्य जीवन और भारतीय संस्कृति के प्रतीकों के लिए प्रकट होता
है। ऐसी अद्भुत, विलक्षण और कालजयी रचनाएँ करने वाले प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ
की विचारधारा से जुड़कर भारतीय संस्कृति और भारतीयता के प्रतीकों को विस्मृत कर
बैठें होंगे, यह स्वीकार करना असंभव है। उल्लेखनीय है कि प्रगतिशील लेखक संघ के
पहले अधिवेशन से पूर्व प्रेमचंद का इस विचारधारा के साथ कोई जुड़ाव नहीं था और इस
अधिवेशन के लगभग छह माह बाद ही प्रेमचंद का असामयिक निधन हो गया। कहना न होगा, कि
प्रेमचंद की सभी रचनाओं को अपने अनुरूप प्रस्तुत करते हुए प्रगतिवाद के झंडाबरदारों
ने प्रेमचंद को अपने खेमे का साहित्यकार घोषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यह
क्रम आज भी देखा जा सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यदि प्रेमचंद जीवित होते,
तो उन्हें भी पंत और नरेंद्र शर्मा की तरह प्रगतिवादी पार्टी से कब का निष्कासित
कर दिया गया होता, या फिर वे जैनेंद्र और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की तरह स्वयं
ही अलग हो गए होते। इसी प्रकार रवींद्रनाथ ठाकुर ने प्रगतिशील लेखक संघ के कोलकाता
अधिवेशन (सन् 1938) की अध्यक्षता की थी। टैगोर का साहित्य, उनकी संगीत-साधना और
उनका जीवन किसी भी प्रकार से प्रगतिवाद की विचारधारा से मेल खाने वाला प्रतीत नहीं
होता। इसी कारण कालांतर में रवींद्रनाथ ठाकुर भी प्रगतिवाद के खेमे से बाहर हो गए।
इस संदर्भ में डॉ. गणपतिचंद्र गुप्त लिखते हैं-
वस्तुतः मुंशी प्रेमचंद
और गुरुदेव टैगोर- दोनों ने ही प्रगतिशीलता को एक व्यापक एवं उदात्त रूप में ही
ग्रहण किया था, जबकि परवर्ती साहित्यकारों ने इसे मार्क्सवाद की संकीर्ण सीमाओं
में अवरुद्ध करके इसे ‘प्रगतिशीलता’ से ‘प्रगतिवाद’ का रूप दे दिया। प्रगतिशीलता
जहाँ किसी वाद-विशेष की सूचक नहीं है। कोई भी विचार, जो समाज की प्रगति में सहायक
होता है, ‘प्रगतिशील’ कहा जा सकता है, जबकि ‘प्रगतिवाद’ का अर्थ विशुद्ध
मार्क्सवादी विचारों से लिया जाता है। इसीलिए ‘प्रगतिवाद’ की परिभाषा करते हुए कहा
गया है कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में
प्रगतिवाद है।7
रूस की जारशाही को नष्ट
करके मार्क्स का जीवन-दर्शन सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर चुका था। इस आकर्षण
ने लंदन से होते हुए भारत में पदार्पण किया। भारत की सनातन परंपरा, जो अतीत के
अनेक उतार-चढ़ावों को देखते-भोगते और विषम परिस्थितियों से जूझते हुए
अखंड-अक्षुण्ण बनी हुई थी, उसमें सेध लगाने के लिए जिस प्रकार प्रगतिवाद अर्थात्
मार्क्सवाद को ‘प्रगतिशीलता’ के आवरण में छिपाकर प्रस्तुत किया गया, उसने अवश्य ही
अनेक बुद्धिजीवियों-साहित्यसेवियों को भ्रमित किया, परंतु भ्रम की यह स्थिति लंबे
समय तक बनी नहीं रह सकी। इस अवधि में ‘प्रगतिवाद’ ने अवश्य ही ऐसा वर्ग तैयार कर लिया
था, जो क्रांति की बात करके, द्वंद्वांत्मक भौतिकवाद की बात करके अपना वर्ग तैयार
करने के प्रयास में सक्रियता के साथ लगा हुआ था। इसी के फलस्वरूप अवसर का लाभ
उठाते हुए ऐसे साहित्यकारों को अपने खेमे में दिखाने का प्रयास ‘प्रगतिवाद’ की
धारा के लोग करने लगे, जिनके साहित्य का उल्लेख करके, जिनके स्वयं के प्रभाव का
वर्णन करके ‘प्रगतिवाद’ की ओर सामान्य जन को, आम पाठकों को आकर्षित किया जा सके।
यह स्थिति राजनीति के
क्षेत्र में भी बनने लगी थी। यहाँ उल्लेख करना होगा, कि इसके लिए सीधा और सरल-सा
रास्ता कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (1929) में ही बन गया था। इस अधिवेशन के
अध्यक्षीय उद्बोधन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को साम्यवादी और प्रजातंत्रवादी
घोषित करते हुए कहा- मैं तो साम्यवादी और प्रजातंत्रवादी हूँ।8
उनके द्वारा ‘साम्यवाद’ शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसे जाने बगैर
पंडित नेहरू के (अंध) अनुयायियों ने साम्यवाद को, और फिर कालांतर में ‘प्रगतिवाद’
को अपना लिया। राजनीति के राजपथ में बिना प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के उन
‘क्रांतिकारियों’ ने स्थान पा लिया था, जिन्हें अनेक सुख-सविधाओं के बीच पूँजीपतियों
और साम्राज्यवादियों जैसे जीवन को जीते हुए सर्वहारा वर्ग की पीड़ाओं और चिंताओं
को कलमबद्ध करने में महारथ हासिल थी। देश के तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दल में
साम्यवादियों की यह घुसपैठ कभी आलोचना का विषय नहीं बन सकी। यह अत्यंत रोचक तथ्य
है कि कांग्रेस की अपनी नीतियों के निर्धारण में भी इनकी दखल होती रही और इसे
स्वीकार किया जाता रहा।
भारतीय समाज-जीवन में
धर्म और आस्था का विशिष्ट महत्त्व रहा है। आध्यात्मिकता के बिना भारतीय समाज की
कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसके एकदम विपरीत
है। इस कारण भारतीय समाज में अपना स्थान बनाने हेतु यह भी आवश्यक था, कि भारतीय
आध्यात्मिकता, धर्म-साधना और आस्थावान जीवन-पद्धति को तोड़ा जाए। इस कारण राजनीति
और साहित्य में अपनी घुसपैठ से उत्साहित होकर ‘प्रगतिवाद’ या ‘द्वंद्वात्मक
भौतिकवाद’ या ‘मार्क्सवाद’ ने धर्म में घुसपैठ का रास्ता खोजना शुरू किया। बौद्धधर्म
के अनात्मवाद, अनीश्वरवाद और विज्ञानवाद ने इस रास्ते को सरल बना दिया। भगवान
बुद्ध द्वारा जिन बातों को अव्याकृत कहा गया था। जिन बातों पर वे मौन रहे थे,
उन्हीं को आधार बनाकर यह प्रचारित-प्रसारित किया जाने लगा, कि बौद्धमत अतीत का, और
मार्क्सवाद वर्तमान का जीवन-दर्शन है। इस कारण बौद्ध धर्म को अंगीकार करना ही
श्रेयस्कर होगा। यह भी प्रचारित किया गया, कि बौद्ध धर्म ही वास्तव में ऐसा धर्म
है, जो सर्वहारा समाज के कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकता है। इसी कारण ‘नव बौद्ध’ का
विचार समाज में न केवल प्रचलित हुआ, वरन् राजनीतिक हथकंडे के रूप में प्रयोग किए
जाने का माध्यम भी बन गया। इसी कारण हजारों वर्षों की उपेक्षा और तिरस्कार की
दुहाई दे-देकर राजनीति की रोटियाँ सेंकीं गईं। हजारों-लाखों का समूह बनाकर लोग
धर्म-परिवर्तन करने लगे।
इस प्रकार साहित्य,
राजनीति और धर्म के क्षेत्र में परजीवी की भाँति सक्रिय होकर भारतीय समाज और
संस्कृति पर कुठाराघात करने का श्रेय द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या प्रगतिवाद या
मार्क्सवाद को जाता है। प्रगतिवादी कविताओं में अनल-गान, अनिल-गान, विप्लव-गान और क्रांति-आह्वान
के ऐसे अनेक स्वर उभरने लगे थे, कि मानों सारा देश अनेक बुराइयों-विकृतियों से भर
गया है और इस क्रांति-गान से एकदम बदल ही जाएगा। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
परजीवी बनकर रह जाने वाली यह क्रांति की धारा धीरे-धीरे अपने पथ से भटकती चली गई
और इसी कारण सबसे पहले साहित्य में इसका स्थान हाशिये पर सिमटकर रह गया। सन् 1950
तक आते-आते यह क्रांति-धारा, यह विप्लव-धारा अपने अवसान की ओर चल पड़ी। राजनीति
में स्वयं कभी अपना स्थान नहीं पाकर भी इस धारा के लोग सत्ता के सुख का स्वाद चखते
रहे और सत्ता के केंद्र तक अपनी पकड़ बनाए रखने वाले ये परजीवी अपनी विकृत
मानसिकता के परिणामस्वरूप अपनी जीवनदायिनी सत्ता-शक्ति को भी ले डूबे। आज धर्म के
क्षेत्र में भी इस परजीवी और विकृत-कुत्सित मानसिकता को जाना-समझा जा रहा है और
वहाँ भी शुद्धि-परिष्कार का क्रम चल पड़ा है। भारतीय समाज-जीवन के संदर्भों में
अप्रासंगिक और अस्वीकार्य इस परजीवी वैचारिकता के अवसान का साक्ष्य बना आज का समय
देख रहा है कि सनातन भारतीय परंपरा को तोड़ने वाले, भारतीय समाज की सहकार और
सद्भाव वाली संस्कृति को विकृत करने की सोच रखने वाले तत्त्व किस प्रकार बहिष्कृत
होते हैं।
संदर्भ-
1.
डॉ. नगेंद्र, प्रगतिवाद और हिंदी साहित्य, साहित्यिक निबंध, संपा. डॉ.
त्रिभुवन सिंह, हिंदी प्रचारक संस्थान, वाराणसी, सं. 1976, पृ. 877,
2.
डॉ. गणपतिचंद्र गुप्त, समाजपरक यथार्थवादी (प्रगतिवादी) काव्य-परंपरा, हिंदी
साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, खंड-2, लोकभारती प्रका. इलाहाबाद, सं. 2010, पृ.
143,
3.
डॉ. नगेंद्र, प्रगतिवाद और हिंदी साहित्य, साहित्यिक निबंध, संपा. डॉ.
त्रिभुवन सिंह, हिंदी प्रचारक संस्थान, वाराणसी, सं. 1976, पृ. 882-883,
4.
वही, पृ. 883,
5.
सुमित्रानंदन पंत, चींटी, युगवाणी, हिंदी कविता डॉट कॉम,
6.
अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, हिंदी विकीपीडिया डॉट आर्ग.,
7.
डॉ. गणपतिचंद्र गुप्त, समाजपरक यथार्थवादी (प्रगतिवादी) काव्य-परंपरा, हिंदी
साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, खंड-2, लोकभारती प्रका. इलाहाबाद, सं. 2010, पृ.
125,
8.
वही, पृ. 128।
(अखिल भारतीय
साहित्य परिषद की पत्रिका साहित्य परिक्रमा के जनवरी-मार्च, 2022 अंक में प्रकाशित)
-डॉ. राहुल
मिश्र