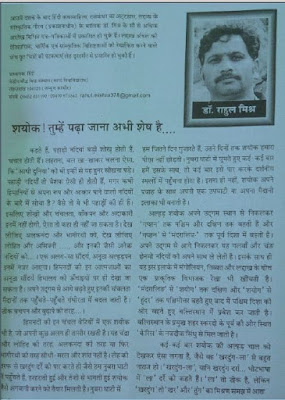सत्तू, तागी और मोमोस जैसे व्यंजनों वाला लद्दाख
मोमोस शब्द और साथ ही इस नाम के व्यंजन का स्वाद आज किसी के लिए अनजाना नहीं है। बड़े-बड़े शहरों में मोमोस बाकायदा ‘इंटरकांटिनेंटल डिशेज़’ परोसने वाले होटलों में भी मिल जाते हैं, और सड़क के किनारे खड़े चाट के ठेलों पर भी ये सुलभ हो जाते हैं। बड़े शहरों की बात अलग ही है, यहाँ तो सबकुछ मिलना सुलभ-सरल है, लेकिन जरा कस्बाई और गँवई-गाँव के खानपान में उतरकर देखिए... आपको आश्चर्य होगा, कि यहाँ टिकिया, समोसा और कुछ आधुनिक होते समय के चाऊमीन-बरगर के साथ मोमोस भी मिल जाएँगे। हिम-आच्छादित लद्दाख का प्यारा और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन- मोमोस... आज देश के कोने-कोने तक पहुँचा हुआ है।
किसी क्षेत्र-विशेष की सांस्कृतिक-सामाजिक पहचान का बड़ा अंग उस
क्षेत्र के प्रचलित व्यंजनों से बनता है। क्षेत्र-विशेष अपनी पहचान गढ़ते समय अपने
व्यंजनों के चटखारों का स्वाद उतारता है। इडली-डोसा का उल्लेख करते ही दक्षिण भारत
का चित्र आँखों के सामने होता है। इसी तरह बुंदेलखंड की बेड़ही-लपसी, पूर्वांचल की
बाटी-चोखा और पंजाब की मक्के दी रोटी-सरसों दा साग अलग-अलग भौगौलिक रंग हमारे
सामने ले आते हैं। देश की सांस्कृतिक विविधता का यह बड़ा अंग है। देश को जोड़ने
वाले व्यंजनों पर अगर बात करें, तो एक अद्भुत रोमांच मन में भर जाता है, जो देश की
विवधता में एकता को अनेक बार हमारे सामने ले आता है। लद्दाख भले ही दुर्गम और जटिल
हो, लोगों के मन में इस बर्फीले रेगिस्तान को लेकर भले ही अनेक भ्रांतियाँ, भय और
आश्चर्यजनक बातें हों; लेकिन लद्दाख के व्यंजनों ने इन मिथों को बखूबी तोड़ा है।
इसी कारण देश के सुदूरवर्ती ग्राम्यांचलों में भी लद्दाखी मोमोस की हनक देखने को मिलती
है।
वैसे तो लद्दाख की पहचान तीन चीजों से रही है, उसके अपने अतीत में.....।
ये तीन चीजें हैं- सत्तू, पट्टू और टट्टू...। आपको यह जानकर निश्चित रूप से
आश्चर्य हो सकता है, कि सत्तू जो है, वह लद्दाख की पहचान में शामिल है, जुड़ा हुआ
है। बाकी दो में से पट्टू, अर्थात् दुशाला लद्दाख की शीत से बचाने के लिए बहुत आवश्यक
है और टट्टू, अर्थात् अश्वों की एक वर्णसंकर प्रजाति लद्दाख की प्राचीन यातायात
व्यवस्था का अभिन्न और प्रमुख अंग रहा है। लद्दाख में यातायात व्यवस्था के अंग के
रूप में याक (चमरी मृग) और यारकंदी ऊँट (दो कूबड़ वाले) भी आते हैं, लेकिन नाम तो
टट्टुओं का ही चलता है। इसका बड़ा कारण यह है, कि स्थानीय आवागमन और सामान ढुलाई
के लिए टट्टू ही अधिकतर उपयोग में आते थे, जबकि यारकंदी ऊँट और याक की भूमिका
प्रायः लंबी और दर्रों को पार करने वाली पहाड़ी यात्राओं में विशेष रूप से होती
थी। ये सारी बातें इसलिए कहीं, कि सत्तू का महत्त्व भी कुछ इसी प्रकार का देखा जा
सकता है, लद्दाख के जटिल जीवन में...।
लद्दाख में जौ की फसल पर्याप्त मात्रा में होती है। इस कारण लद्दाख
में जौ का सत्तू चलन में है। भारत के मैदानी क्षेत्रों, जैसे- मध्यप्रदेश,
उत्तरप्रदेश और बिहार आदि में चने का सत्तू चलता है। लद्दाख में चने की पैदावार नहीं
है, लेकिन सत्तू बनाने की विधि है, सत्तू भी है... भले ही जौ का ही क्यों न हो..।
जौ का सत्तू न केवल पौष्टिक होता है, वरन् इसकी तासीर गर्म होती है, जबकि चने के
सत्तू की तासीर ठंडी होती है। यह भी एक बड़ा कारण लद्दाख में जौ के सत्तू के चलन के
पीछे है। यह देखन बहुत रोचक है, कि सत्तू, जिसे लद्दाखी भाषा में ‘फे’ बोलते हैं,
उसका प्रयोग कई तरीके से रसोईघर और अतिथिगृह में होता है। कुछ व्यंजनों में इसका
उपयोग किया जाता है, पूजा-पाठ में भी इसका उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त यह सबसे
अधिक चाय के साथ खाया या पिया जाता है।
लद्दाख में पानी पीना किसी चुनौती से कम नहीं, इस कारण भारत के
मैदानी क्षेत्रों की तरह यहाँ पर अतिथियों के आगमन पर उन्हें पानी के लिए नहीं पूछा जाता है, चाय के
लिए पूछा जाता है। चाय भी कई तरह की...., जैसे- गुरगुर चाय, लिप्टन चाय, ग्रीन टी
और कहवा आदि। ग्रीन टी और कहवा से तो सभी परिचित होंगे, वैसे परिचित तो लिप्टन चाय
से भी होंगे.... भ्रम केवल नाम के कारण हो सकता है। लिप्टन चाय दरअसल दूध वाली
मीठी या शर्करामुक्त चाय के लिए प्रयोग होने वाला नाम है। इस नाम के माध्यम से
लद्दाखी लोग चाय का एक भेद गढ़कर अतिथि को उसके चाय-चयन में मदद दे देते हैं। सबसे
अधिक प्रचलित और प्रिय गुरगुर चाय है, लद्दाख में। यह पसंद तिब्बत तक बिखरी हुई
है..., कह सकते हैं, कि समूचे हिमालयी परिक्षेत्र में गुरगुर चाय का चलन है।
गुरगुर चाय वस्तुतः मक्खन डालकर बनाई गई
नमकीन चाय है। इसके अपना नाम भी इसके बनाने में होने वाली ध्वनि से मिला है। लंबे
बेलनाकार बरतन में मथानी जैसे डंडे से मथकर यह बनती है, और मथते समय गुरगुर की
आवाज होती है। थोड़ी-सी चायपत्ती और मक्खन से बनी गुरगुर चाय में अनूठा-सा सोंधापन
होता है। यह शरीर में नमक और पानी की मात्रा संतुलित करती है। गुरगुर चाय की
प्याली के साथ सत्तू भी परोसा जाता है। अतिथिगण चाय की प्याली में सत्तू घोलकर या
तो पी जाते हैं, या फिर खा लेते हैं। सत्तू ऐसा आहार है, जिसे आप तैयार खाद्य या ‘फास्ट
फूड’ की श्रेणी में भी आसानी से रख सकते हैं। किसी भी यात्रा के लिए यह साथ ले जाने
वाला सर्वोत्तम आहार है। कहीं पर भी खाया जा सकता है, कैसे भी खाया जा सकता है। मध्यभारत
में तो सत्तू-नमक लेकर ढूँढ़ना... जैसे मुहावरे भी बने है। सत्तू यात्राओं के लिए
बहुत उपयुक्त रहा है, विशेषकर जटिल-कठिन यात्राओं के लिए...।
लद्दाख यात्राओं के मार्ग का पड़ाव जैसा है।
लद्दाख के ऊपरी हिस्से से होकर रेशम मार्ग निकलता है। लद्दाख की नुबरा घाटी रेशम
मार्ग के यात्रियों के लिए एक आरामगाह जैसी रही है। इसके साथ ही भारत के अन्य
हिस्सों के लिए उतरने वाले संपर्क मार्गों के कारण लद्दाख एक बड़े व्यापारिक
केंद्र व ठहराव के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहा है। होशियारपुर के अनेक
व्यापारियों के ठिकाने आज भी लेह में देखे जा सकते हैं। गुरु नानक अपनी यात्राओं
के क्रम में लद्दाख भी पधारे थे। लेह के निकट गुरुद्वारा दातून साहिब और
लेह-श्रीनगर राजमार्ग पर गुरुद्वारा पत्थरसाहिब उनकी यात्रा की अविस्मरणीय गाथा को
आज भी गाते हैं।
एक समय ऐसा भी था, जब लेह बाजार में मध्य
एशिया के हर हिस्से का प्रतिनिधित्व दिखाई देता था; व्यापारियों, क्रेता-विक्रेताओं,
पहनावों और बिकते व्यंजनों के रूप में...। लेह बाजार में गुरुद्वारा दातून साहिब
के पास ही नहीं, प्रायः पूरे लद्दाख में एक वर्ग ऐसा मिलेगा, जो तंदूरी रोटी
बनाने-बेचने का काम करता है। इन्हें स्थानीय भाषा में नानवाई कहते हैं। इनके
द्वारा बनाई तंदूरी रोटी लद्दाखी भाषा में ‘तागी’ कही जाती है। यह तागी कब रेशम
मार्ग से उतरकर लद्दाख की ‘तागी’ और फिर पंजाब की ‘तंदूरी’ बनकर सारे देश और
दुनिया में फैली...., जानना बहुत रोचक और रोमांचकारी होगा।
रेशम मार्ग पर चलने वाले यात्रियों और व्यापारियों
के लिए दाना-पानी कितना जटिल रहा होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। रेशम मार्ग
में यात्रा करने के लिए पूरा का पूरा लाव-लश्कर होता था, जिसमें दो कूबड़ वाले
ऊँटों पर चमड़े के बने थैलों में पानी, तागी या तंदूरी रोटी आदि के चलते-फिरते
भंडार भी होते थे। इनके साथ ही समोसा जैसे व्यंजन भी होते थे, जो आटे के अंदर तीखा-चटपटा
मसाला भरकर बनाए जाते थे। समोसा की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, ऐसा कह सकते हैं। रेशम
मार्ग केवल व्यापार का ही रास्ता नहीं था, बल्कि दर्शन-चिंतन-वैचारिकता की अनेक
बातें भी इस मार्ग से आती जाती रहीं हैं। अनेक अध्येताओं ने इस रास्ते से चलकर
ज्ञान की खोज की है। संस्कृतियों के आदान-प्रदान के साथ ही खान-पान की आदते और
व्यंजन भी रेशम मार्ग से आए-गए हैं। और इन सबका प्रभाव आज भी लद्दाख में देखा जा
सकता है। लद्दाख को यूँ ही नहीं मध्य एशिया का बड़ा केंद्र कहा जाता...।
प्रायः भौगोलिक
परिस्थितियाँ और जलवायु के कारक क्षेत्र-विशेष के आहार-विहार को प्रभावित करते
हैं। लद्दाख में यह पक्ष प्रमुख रूप से दिखता है। इसी कारण लद्दाखी व्यंजन देश के
अन्य भागों के व्यंजनों से अलग बनते हैं। लद्दाखी व्यंजन स्थानीय आवश्यकता के
अनुसार प्रायः पर्याप्त तरल होते हैं। अकसर सूप तरलता को बढ़ाने का काम करते हैं।
मैदानी क्षेत्रों में मोमोस को भले ही चटनी के साथ खाने का चलन हो, लेकिन लद्दाख
में मोमोस सूप के साथ ही खाए जाते हैं। मोमोस के अतिरिक्त थुक्पा में भी पर्याप्त
सूप होता है। थुक्पा व्यंजन में मोटी सेवइयाँ जैसी होती हैं, जिन्हें खूब रसेदार सूप
में डालकर पकाया जाता है, और गरम-गरम पी लिया जाता है। इससे शरीर में गरमी भी आती
है, और पानी की कमी भी साथ-साथ पूरी होती जाती है। ‘स्क्यू’ भी कुछ इसी तरह का
व्यंजन होता है। इसमें ढेर सारी सब्जियाँ- पालक, मंगोल, लाल मटर आदि डालकर खूब तरल
करके पकाया जाता है, और खौलती हुई तरल सब्जी में आटे के गोल-चौकोर टुकड़े जैसे
डालकर उबाला जाता है। इसे भी रसेदार बनाते हैं और इसे भी सूप की तरह से पीते हुए
खाया जाता है।
खोलक एकदम अलग तरह का व्यंजन है। लद्दाख में
चपातियाँ बनाने का विधान नहीं है। चपाती के रूप में अगर कहें, तो ‘तागी’ ही है, जिसका
उल्लेख पूर्व में किया गया है। एक रोचक बात ‘तागी’ के बारे में बताना यहाँ आवश्यक
लगती है। लद्दाख में एक कहावत कही जाती है- ‘बेचारा रोटी खाकर जिंदा है..।’ यह कहावत
गरीब-दीन-हीन व्यक्ति के लिए कही जाती है। लद्दाख में चावल विशिष्ट और कुलीन वर्ग
का आहार माना जाता था। लद्दाख में चावल पैदा नहीं होता था, जिस कारण चावल बहुत
महँगा बिकता था। दूसरी तरफ नानवाई की रोटियाँ सहज सुलभ थीं, हर वर्ग के व्यक्ति के
लिए..। आज स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन अतीत की यादें जीवंत हैं। हम बात कर रहे थे,
लद्दाखी व्यंजन खोलक की..। यह एक तरह से चपाती का ही रूप है, लेकिन इसे सीधे आँच
में नहीं पकाया जाता। मैदा या आटा को सानकर उसका कलात्मक लड्डू जैसा आकार बनाकर
भाप में पकाया जाता है। फिर उसे दाल में डालकर या सब्जी के साथ खाया जाता है।
लद्दाख की जलवायु के अनुसार यहाँ के प्रायः
सभी व्यंजन कम मसालेदार और भाप में पके हुए होते हैं। इनको पकाने के लिए अलग तरह
के बरतन भी होते हैं। वैसे लद्दाखी रसोई भी कम कलात्मक नहीं होती। लद्दाखी घरों
में रसोई केवल खाना पकाने के लिए नहीं होती, वरन् खाना खाने और घंटों बैठकर गपशप
करने के लिए भी होती है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लद्दाख और तिब्बत की अपनी
यात्राओं के साथ यहाँ के रसोईघरों का भी रोचक वर्णन किया है। वे यह भी लिखते हैं,
कि बाहरी व्यक्ति के लिए रसोई तक पहुँचना कठिन नहीं होता। रसोईघर में चूल्हा कुछ
इस तरह का होता है, कि उसके निकट बैठकर शीत से बचाव किया जा सकता है। इस तरह पूरा
परिवार और अतिथिगण भी रसोई में बैठकर गरमागरम भोजन का आनंद ले सकते हैं, शीत से
स्वयं को बचाते हुए। यह व्यवस्था एक तरह से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए जीवन जीने
की कला भी सिखाती है।
विश्वग्राम की संकल्पना ने सारी दुनिया को
एक जगह पर समेट दिया है। जिस तरह मोमोस लद्दाख से निकलकर सुदूरवर्ती गाँवों तक
पहुँचे हैं, उसी तरह से चोखा-बाटी, इडली-डोसा, जलेबी-टिकिया आदि लद्दाख में भी
सुलभ हैं। इतना ही नहीं लद्दाख के बड़े होटलों के साथ ही छोटे-छोटे होटलों और रेस्टोरेंट्स
में ‘इंटरकांटिनेंटल डिशेज़’ भी खूब मिलती हैं। लद्दाख उभरते हुए पर्यटन केंद्र के
रूप में देश ही नहीं विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। इस कारण देश-दुनिया के
पर्यटकों के साथ देश-दुनिया की खान-पान की आदतें और व्यंजन भी लद्दाख पहुँचे हैं।
आज के समय में सत्तू लद्दाख के दूर-दराज के गाँवों में सरलता से मिल सकता है, अपेक्षाकृत
लद्दाख के शहरी क्षेत्रों के...। आधुनिकता
ने बहुत कुछ बदला है। यह बदलाव खान-पान में भी आया है। यह सांस्कृतिक संक्रमण का
समय है। लद्दाख के ठंड से ठिठुरते समय में बैठकर मसाला डोसा खाना एकदम अलग अनुभव
देता है। किसी गाँव के चाट के ठेले में खड़े होकर मोमोस खाना भी अलग ही लगता है। अगर
गहरे उतरकर सोचें, तो कई-कई बार यह अनुभूत होता है, कि हम व्यंजन नहीं, देश को एक
सूत्र में पिरोने वाले सूत्रों का सुख व आनंद अपने अंदर उतार रहे हैं।
-राहुल मिश्र (आचार्य अनामय)
(कश्फ, अर्धवार्षिकी, संयुक्तांक दिसंबर, 2021 से जून, 2022, वर्ष- 20-21, संपादक- डॉ. विनोद तनेजा, अमृतसर में प्रकाशित)